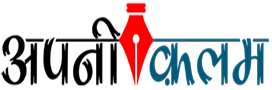हकीमी से शायरी के मैदान में उतरे मजरूह सुल्तानपुरी ने गंभीर गीतों से लेकर ‘आज मैं ऊपर आसमां नीचे’ जैसे बेहद संगीतमय गाने लिख कर दिखा दिया कि फिल्मी गीतों में भी इन्द्रधनुष के रंग भरे जा सकते हैं। दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजे गए मजरूह के बारे में कहा जाता है कि वह शुरू से लेकर अंत तक शायर ही रहे। असरार उल हुसैन खान उनका असली नाम था और एक दौर में उन्हें एक उम्दा हकीम के रूप में जाना जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि सुल्तानपुर में मुशायरा हुआ और हकीम साहब मंच पर आ गए। उन्होंने एक मिसरा सुनाया और मतला तक आते-आते सुनने वालों ने हकीम साहब की प्रतिभा का लोहा मान लिया। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। हकीम साहब ने अपनी हकीमी को अलविदा कहा और शायरी के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपना जमा जमाया हकीम का पेशा एक किनारे छोडा और नए सफर का आगाज किया। इस सफर ने हकीम साहब को एक नए नाम से नवाजा जिसे सारी दुनिया मजरूह सुल्तानपुरी के रूप में जानती है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अक्तूबर वर्ष 1919 को जन्मे मजरूह सुल्तानपुरी ने इसके बाद कभी पीछे मुडकर नहीं देखा औरर शब्दों का ऐसा जादू चलाया कि सुनने वालों के कान खुले होते थे और आंखें बंद हो जाती थीं।
शब्दों के जादूगर मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में गजलकार राहत इंदौरी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब शायरी दरबारों और कोठों की तंग गलियों में सिमटी हुई थी। लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने शायरी को न केवल आजाद किया बल्कि उसे एक नया आयाम भी दिया। अपने गीतों और गजलों से न जाने कितने दिलों में अरमान जगाने वाले राहत इंदौरी ने कहा कि मजरूह सुल्तानपुरी तरक्की पसंद खूबसूरत नज्मों में माहिर थे। उन्होंने शब्दों को गजल में पिरोकर आजादी और बराबरी का पैगाम दिया।
मजरूह सुल्तानपुरी को वर्ष 1993 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। वह ऐसे पहले गीतकार हैं जिन्हें यह सम्मान हासिल हुआ। इन दिनों युवाअ¨ं में फिल्म बचना ए हसीनों का शीर्षक गीत बेहद लोकप्रिय हुआ है। यह गीत मूलतः मजरूह सुल्तानपुरी ने ही वर्ष 1977 में आई फिल्म ‘हम किसी से कम नहीं’ के लिए लिखा था। तब राहुल देव बर्मन के संगीत में किशार कुमार ने इस गीत को अपनी आवाज से सजाया था। –
मजरूह की रचनाएं
निगाहे-साकी-ए- नामहरबाँ ये क्या जाने
कि टूट जाते हैं, खुद दिल के साथ पैमाने
मिली जब उनसे नजर, बस रहा था एक जहाँ
हटी निगाह तो चरों तरफ थे वीराने
हयात, लग्जशे-पैहम का नाम है साकी
लबों से जाम लगा भी सकूँ, खुदा जाने
वो तक रहे थे, हमीं हंस के पी गए आंसू
वो सुन रहे थे, हमीं कह सके न अफसाने
ये आग और नहीं, दिल की आग है नादाँ
चिराग हो कि न हो, जल बुझेंगे परवाने
फरेबे-साकी-ए-महफिल न पूछिये ‘मजरूह’
शराब एक है, बदले हुए हैं पैमाने
० ० ०
खत्मे-शोरे-तूफाँ था, दूर थी सियाही भी
दम के दम में अफसान: थी, मिनी तबाही भी
इल्तफात समझूँ या बेरूख़ी कहूँ इस को
रह गई खलिश बन कर उसकी कमनिगाही भी
याद कर वो दिन जिस दिन तिरी सख़्तगीरी पर
अश्क भर के उठी थी मेरी बेगुनाही भी
शम्अ भी, उजाला भी मैं ही अपनी महफिल का
मैं ही अपनी मंजिल का राहबर भी, राही भी
गुम्बदों से पलटी है अपनी ही सदा ‘मजरूह’
मस्जिदों में की जाके मैंने दादख़्वाही भी