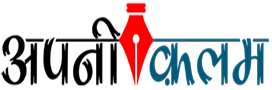मुगलिया दौर के मशहूर बादशाह शाहजहां की बेटी और औंरगजेब की सगी बहन थी- जहांआरा। शाहजहां की चहेती बेगम मुमताज की कोख से उसकी पैदाइश 1 अप्रैल 1614 ई. को हुई। वह ऐसा वक्त था जब उसके वालिद शाहजादा खुर्रम की हैसियत से, शाही हुक्म की वजह से उदयपुर के राणा अमर सिंह से जंग में मशगूल थे।
शाही ठाट-बाट के बीच भी जहांआरा ने अपना काफी वक्त पीरों-दरवेशों के दीदार और खिदमत में गुजरा। उन्होंने अपनी सवाने हयात के बतौर दो बहुत खास किताबें लिखीं, जिनमें सूफी दरवेशों, वलियों वगैरह से मुताल्लिक बातें लिखी हैं। इनमें से एक किताब का नाम है ’’मूनिसुल-अरवाह‘‘, इसमें उसने सूफियों के चिश्तिया-मसलक के बुजुर्गों के कौल तथा उनसे जुडी आपबीती, वाकेआत का जिक्र किया गया है। उनकी दूसरी किताब है -’साहिबिया‘।
इसकी एक हाथ की लिखी कापी हैदराबाद के सरकारी म्युजियम में और दूसरी कापी कुतुबखाना आसिफिया में हिफाजत से रखी हुई हैं। अपनी इस किताब में जहांआरा ने उन बातों का संक्षेप में बयान किया है जो उसके आध्यात्मिक जिंदगी से जुडी थीं। उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वह चिश्तिया पंथ में दीक्षित हों, पर कुछ वजहों से उनकी यह ख्वाहिश पूरी न हो सकी। उसने अपने भाई दारा शिकोह से भी (जो एक आलिम, फाजिल और जानकार था) बहुत कुछ इल्म हासिल किया था और उसी के मश्विरे से एक बुजुर्ग की शार्गिद बनीं। उस वाक्ये का जिक्र अपनी किताब ‘साहिबिया‘ में किया है। जिसका हिन्दी में तर्जुमा यहां पेश किया जाता हैः-
तोरे चरन लागी अब कित जावां
‘‘ जब मैं 20 साल की थी तभी से चिश्तिया बुजुर्गों से मुझे बेहद लगाव और उन्स हो गया था। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के लिए बहुत प्यार ही मेरी सबसे बडी पूंजी है। कुछ साल पहले मैं उनके रोजे मुबारक का दीदार हासिल कर चुकी हूं। उनके लिए मेरी अकीदत और लगन दिन ब दिन बढती ही गयी है। अब अल्लाह ने मेरे दिल में चाह पैदा की है। अपने भाई दारा शिकोह के साथ से जो आरिफे कमाल हैं, यह चाह बहुत ज्यादा बढ गई है।
जब मैं अपने वालिद के साथ लाहौर पहुंची तो मरेा भाई मेरे साथ था। उसी साल मेरे वालिद ने भाई को काबुल की तरफ भेज दिया। भाई को विदा करते वक्त मैं बहुत रोई। उस वक्त भाई ने मुझे ’नग्मातुउन्स‘ को पढने की ताकीद की। मैंने हमेशा उस किताब को पढती रही और उससे काफी फायदे हासिल किये।
मेरे वालिद ने काबुल को फतेह करने का इरादा किया। मेरे भाई ने खतों के जरिये मुझे दो बुजुर्गों-दरवेशों के बारे में जानकारी पहुंचाई। उनमें से एक तो शैख शाह दूल्हा दरियाई थे, जो गुजरात (खुर्द) में रहा करते थे। दूसरे हाजी अब्दुल्लाह थे, जो तालोजलाल खखोड में तन्हाई में जिंदगी गुजार रहे थे।
जब हमारी सवारी गुजरात पहुंची तो मैंने अपने एक खादिम के जरिये शाह दूल्हा के पास तोहफे भेजे और उनसे गुजारिश की। मगर जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। जब हम तालजलाल खखोड पहुंचे तो मैंने हाजी साहब की भी नजरे इनायत हासिल करनी चाही। मैंने उन्हें जो तोहफा भेजा, उसे उन्होंने लौटा दिया और अपनी तरफ से मेरे लिए एक तस्बीह (माला) और नमाज पढने का मुसल्ला भेजा, जो उन्होंने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। वे मेहनत से कमाई रोजी पर गुजर-बसर करते थे और उसी कमाई में से तैयार दो रोटियां भी उन्होेंने मुझे भेजीं। तब मैंने उन्हें रोटियों का एक टुकडा खाया तो मेरी रूह रोशन हो गयी। मुझे बहुत रूहानी सुकून तथा खुशी हासिल हुई। वे दो रोटियां मैंने तीन दिनों तक खुद खायीं और अपनी नौकरानियों को भी खिलायीं।
यहां से हमारा काफिला हसन अब्दला पहुंचा, जहां हमारी मुलाकात अपने भाई से हुई। उसने मुझे दरवेश-बुजुर्गों के जिंदगी के बारे में पढने की सलाह दी।
जब हम काबुल पहुंचे तो कुछ दिन बाद भाई भी आ पहुंचे और वालिद साहब ने बल्ख को फतेह करने का अपना इरादा छोड दिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए शुकराने की नफिल नमाजें पढीं।
अब वालिद साहब ने लाहौर का इरादा किया और हम रजब सन् 1029 हिजरी को लाहौर शहर में दाखिल हुये। लाहौर में बडे-बडे दरवेश व औलिया रहते थे। मैंने चिश्तिया दरवेशों की तलाश शुरू की, मगर मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिली। मुल्ला ख्वाजा बहारी की शोहरत सभी तरफ फैली हुई थी, लेकिन वह किसी को शार्गिद नहीं बनाते थे। मैं इस पर थोडा सा परेशान हुई पर मेरी तलाश जारी रही। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि किसी पूरे कामिल बुजुर्ग की शार्गिदी हासिल कर लूं, चाहे वह किसी भी फिरके से हो, क्योंकि अब मेरी उम्र 27 वर्ष की हो चुकी थी। इसी साल मेरे वालिद ने कश्मीर का इरादा किया।मैं भी उनके साथ थी।
जिल्हिज के महीने में जब हम कश्मीर पहुंचे तो मालूम हुआ कि हजरत शेख मियां पीर के खलीफा मुल्ला शाह बदख्शी कश्मीर में हैं। मेरे भाई को उनसे बहुत लगाव है। उसने मुल्ला साहब की इतनी तारीफ की कि मेरा दिल उनके लिए अकीदत से भर गया। मैंने बहुत ही अकीदतमंदी के साथ उनको एक खत लिखा और तोहफा पहुंचाने के लिए अपने हाथ से साग तैयार किया। खुद ही रोटियां पकाईं और अपने एक खादिम के हाथ उनकी खिदमत में पहुंचाईं। खतों का जवाब उन्होंने कुछ भी नहीं दिया और कहलाया -’’ बादशाहों और दुनियादारों से हमें क्या काम।‘‘ मगर मैं नाउम्मीद नहीं हुई और उन्हें बराबर पुरइसरार खत लिखती रही। जब उन्होंने मुझे सच की तलाश में वाकई सच्ची और मजबूत इरादे का पाया तो मेरे कुछ खतों के जवाब भी दिये। मैं उम्मीद और खुशी से भर उठी।
एक दिन मैंने छुप कर उन्हें देख भी लिया। नूर से जगमगाता उनका चेहरा देख कर मेरी आंखें चैंधियां गईंं। मैंने अपने भाई के जरिये उनके हाथ में अपना हाथ देकर उनकी मुरीदी हासिल कर ली। भाई के जरिये उन्होंने मुझे कादरिया पंथ के तरीके से इबादत और रियाजत करने का हुक्म दिया। पीर साहब को देखने के लिए मुझे मेरे भाई ने मुझे उनकी एक तस्वीर भी दी, जिसे मैं बहुत ही अकीदत और इज्जत के साथ देखती थी।
मेरे भाई ने सबसे पहले मुझे कादरिया सिलसिले की मुरीदी दिलाई। मेरे पीर व मुर्शिद की छवि, हजरत मुहम्मद के चार यार और अन्य दरवेशों-वलियों की इबादत और रियाजत का तरीका सिखाया। मैंने गुस्ल किया, नया जोडा पहना और रोजा रखा और शाम को रोजा उसी चीज से खोला जो मेरे पीर व मुर्शिद ने मेरे लिये ही भेजी थीं।
मेरे पीरे-तरीकत हजरत मुल्ला मुहम्मद सईद के यहां खाना खाया करते थे। मैंने भी उन्हीं के यहां से खाना मंगा कर खाया और घर की मस्जिद में आधी रात तक बैठी तहज्जुद की नमाज पढकर लौटी और फिर काबे की तरफ मुंह करके बैठ गई। शाह साहब की छवि का ध्यान किया और हजरत मुहम्मद सल्ल., उनके सहाबा (साथी) व और दूसरे दरवेशों का तसव्वुर कर ध्यान में खो गई।
उस वक्त में थोडी पशोपेश में थी कि मैंने चिश्तिया सिलसिले के बजाये कादिरिया सिलसिले में मुरीदी ली है। इसलिए शायद मुझे रूहानी फायदा न मिल पाये। तभी मैंने एक ऐसी हालत को मेहसूस किया जो न सोने की थी न जागने की। उसी अजीबो गरीब हालत में मैंने हजरत मुहम्मद सल्ल. की पाक महफिल का नजारा देखा, जिसमें बहुत से सहाबा और दरवेश शामिल थे और मुल्ला शाह भी उसमें मौजूद थे। मैंने देखा कि जब उन्होंने अपना सिर हजरत मुहम्मद सल्ल. के कदमों में रखा तो हजरत ने फरमाया कि – ’’मुल्ला शाह! तूने तैमूरी चिराग को रोशन करा दिया है।‘‘ जब यह हालत खत्म हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जाग गई हूं। जो बात मैंने सुनीं थीं उससे मेरा रोयां-रोयां खिल रहा था। मैंने अल्लाह तआला का बहुत शुक्र अदा किया।
कमोबेश छह महीने तक हम कश्मीर में रहे। मैं अपने पीरो-मुर्शिद को चिट्ठी लिखती और वे मुझे जवाब देने की इनायत फरमाते। हालांकि वे तो दुनिया के तमाम बखेडों से आजाद थे, मगर मैं अकीदत में उनकी खिदमत में तरह-तरह के इत्र और किस्म-किस्म के लजीज खाने अपने हाथों से पका कर भेजा करती थी। इस शागिर्दी के बाद मेरी जिंदगी में एक बडा इंकलाब आ गया था। इससे पहले भी मैं गैर शरयी बातों से बचती थी, अब और ज्यादा होशियार रहने लगी।
जब हम कश्मीर से रवाना होने वाले थे, तो तीन दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने उनसे वह दुपट्टा मांगा जो वह अपने कंधों पर रखा करते थे। उन्होंने वह दुपट्टा मुझे इनायत फरमा दिया। सुबह को जब मैं नींद से जागी तो मैंने सोचा कि उनको अर्जी लिखूं और वह दुपट्टा मांग लूं। अभी मैं यह सोच ही रही थी कि मेरा वह खादिम, जो हमेशा उनकी खिदमत में आया-जाया करता था, मेरे पास हाजिर हुआ और बोला-’’कल शाम मैं शाह साहब की खिदमत में पहुंचा था। मगरिब की नमाज के बाद उन्होंने अपने कंधे से दुपट्टा उतारा और मुझे देकर फरमाया-‘इसे उनके लिए ले जा।‘ मैंने दुपट्टा सेवक के हाथ से ले लिया। आंखों से लगाया और बहुत ज्यादा रूहानी खुशी मुझे हासिल हुई।
मैं दो बार उनके दीदार से सरफराज हुई। पहली बार का जिक्र में इससे पहले कर चुकी हूं। दूसरी बार उनका दीदार मुझे उस दिन मिला, जब मैं कश्मीर से लाहौर आ रही थी। मैंने उनकी खिदमत में अर्जी लिख भेजी-’’चूंकि मैं अब कश्मीर से जा रही हूं, इसलिए आप मेहरबानी फरमायें, ताकि मैं आपके दीदार कर सकूं। उन्होंने मेरी गुजारिश को कुबूल कर लिया। वह उस रास्ते पर, जहां से मेरी सवारी गुजरने वाली थी, एक पेड के नीचे आकर बैठ गये। मैं परदेदार हौदे में हाथी पर सवार थी। जब मैं उस पेड के पास पहुंची तो अदब से खडी हो गई और उनके पूरे जमाल का दीदार कर खुश हुई। उस वक्त उनकी खिदमत में तीन लोग हाजिर थे। एक तो मुहम्मद हलीम थे, जिन्हें वह बहुत मुहब्ब्त करते थे, दो और लोगों में कश्मीरी खादिम थे, जिनके नाम हसन और खिज्र थे। वे उनके पीछे खडे थे। उनमें से एक ने घोडा पकड रखा था।
मैंने अपने खादिम के जरिये कुछ तोहफे और शीशा अर्के गुलाब उनकी खिदमत में पहुंचाया और ताकीद की कि अर्के गुलाब को हजरत से चखवा कर वापस ले आये। ऐसा ही किया गया। इसके बाद वह घोडे पर सवार होकर अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गये। मैंने भी वहां से विदा ली।‘‘ क्रमशः