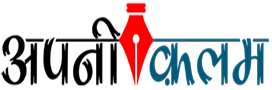दूसरी किश्तः-
मेरी झोली भर दे आयी हूं दूर से
शाही महलों में पैदा हुई एक बादशाह की लाडली बेटी जो शाही ठाट-बाट के बीच रहती-बसती थी, तन से शहजादी होते हुए भी दिल और जान से इस दरजे की मजहब की इबादत गुजार भी हो सकती है, यह कम ही लोग जानते होंगे। जहांआरा की असली जिंदगी, किरदार व बर्ताव वाकई ऐसा ही था। उसकी इस इबादत गुजार जिंदगी से मुताल्लिक कई तस्वीरें और हमें उसके लिखे दूसरे यादगार से भरपूर किताबें ’’मूनिसुलअरवाह‘‘ में नजर आती हैं। उस किताब में उसकी बयान की हुई एक रूहानी यादगार इस तरह से है‘ः-
’’आमतौर पर मुझे बेगम साहिबा के लकब से पुकारा जाता है। मैं अपने वालिद (शाहजहां) के औलादांे में सबसे बडी हूं। जब किसमत के उठाव और अल्लाह की मेहरबानी से मैंने अपने वालिद के साथ आगरा से अजमेर शरीफ की पाक जमीन की तरफ चली तो सन् 1053 हिजरी शाबान महीने से रमजान महीने की 15 वीं तारीख जुमे के दिन तक अनासागर ताल के किनारे बनी शाही इमारतों में रूकी रही। खुदा ने मुझे नेक तौफीक भी दी कि मैं रोजाना पडाव में दो रकअत नफिल नमाज अदा करूं। एक दफा सूरह यासीन एवं सूरह फातिहा पूरे भरोसे व अकीदत में साथ पढती और उसका सवाब हजरत पीर दस्तगीर ख्वाजा मुईनउद्दीन चिश्ती की पाक रूह की ओर भेंट करती। उन थोडे से दिनों में, जो मैंने अजमेर की उन इमारतों में गुजारे, अदब और अकीदत की वजह से मैंने पलंग पर सोना छोड दिया था। मैं उनके पाक रोजे की तरफ पैर करके तो या पीठ करके भी नहीं लेटती थी।
हजरत पीर दस्तगीर की बरकत और जन्नत निशान उस पाक जमीन के असर से मुझे तो दिल की खुशी व रूहानी सुकून हासिल हुई। उसे अल्फाजों में मैं बयान नहीं कर सकती। एक रात मैंने मीलाद और रौशनी (चिरागां) भी कराया। जितनी भी खिदमत और इबादत मुझसे बन सकी करने में मैंने कोई कसर नहीं उठा रखी। कोई कमी नहीं की। न आगे ऐसा कर सकूंगी। खुदा का शुक्र और अहसान है कि रमजान महीने की 16 वीं तारीख को जुमेरात के दिन मुझे उनके दीदार की खुशकिस्मती हासिल हुई।
उसके बाद एक बार फिर उनके रोजे के दीदार को पहुंची। अपने मुंह को उस पाक जमीन की पाक धूल से रगडा, दरवाजे से बीच गुबंद तक नंगे पैर, जमीन को चूमते हुए पहुंची। जब मैं गुबंद के अंदर दाखिल हुई तो सात बार अपने पीर और हादी की मजारे मुुबारक के चक्कर लगाये। वहां की खाक अपनी आंखों की पलकों से बुहारी। उस वक्त ऐसी डूबी और ऐसी खुशी हासिल हुई जिसका बयान नहीं किया जा सकता। खुशी के मारे मैं हैरान थी कि उस वक्त क्या करूं और कया कहूं। मैंने अपने हाथों से मजार पर इत्र मला और फूलों की चादर, जो मैं खुद तैयार करके अपने सिर पर लेकर आई थी। मजार मुबारक पर चढायी। गुंबद में बैठ कर सूरह यासीन और सूरह फातिहा को पढ कर उसका सवाब उनकी पाक रूह को पेश किया। फिर संगमरमर की शाही मस्जिद में बैठ कर जो कि इस ’हकीर‘ के वालिद ने बनवाई है, जाकर नमाज अदा की।
मगरिब के वक्त तक वहीं रही। मजार पर शमा जलाई और वहीं के चार चुल्लू पानी से रोजा इफ्तार किया। वहां की ऐसी सांझ देखी जो सुबह से कहीं बढ-चढ कर थी। अगर मेरे बस में होता तो हमेशा उनके मजार पर ही रहती। उनकी नजरे इनायत चाहती, उनकी इनायत उसी कोने में थी। मैं और भी खिदमत करना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि ऐसी पाक जमीन को छोड कर घर लौट आऊं, मगर मैं मजबूर थी।
आखिरकार आंसू भरी आंखों और भारी दिल के साथ मैं अपनी बेबसी पर हजार अफसोस करती हुई, उस दरगाह से रूखसत होकर अपने ठिकाने पर लौट आई। उस सारी रात एक अजीब सी बैचेनी मुझ पर छायी रही। उससे अगली सुबह जुमे का दिन था। वालिद साहब ने वहां से कूच किया और वापस आगरा की तरफ चल पडे।‘‘
निजामुद्दीन औलिया के पास
चिश्तिया सिलसिले के दरवेशों से बेपनाह अकीदत की वजह से जहांआरा ने मरने के बाद उन्हें में से किसी बुजुर्ग के साये में अपने आपको दफन करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसलिए उसने दिल्ली के मशहूर सूफी-संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में दफन होने का इंतजाम कर लिया था। उसने एक जगह पसंद करके वहां के खादिमों और मुजाबिरों केा अपना सारा माल-असबाब देकर, जो कि तीन करोड रूपये की कीमत का था, वह जगह खरीद ली थी और अपने सामने ही कब्र भी बनवा ली थी। 11 जनवरी सन् 1681 ई. में जब उनका इंतकाल हुआ तो उसे यहीं दफन किया गया। हजरत अमीर खुसरो की मजार के नजदीक बनी जहांआरा की कब्र सिर से पैर तक संगमरमर सग बनी हुई है और बेहद नफीस व खूबसूरत जालियां इसकी खासियत हैं। जहांआरा की ख्वाहिश के मुताबिक कब्र पर कोई छत नहीं बनाई गयी, यानी इस इबादत गुजर की खुले आसामन के नीचे बनी कब्र पर मानो आसमान से बरकतें बरसती रहती हैं।