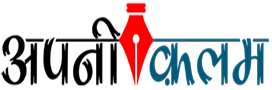किस्सा सच्चा है दिल्ली के एक हाई-फाई कॉलेज में एक कन्या दूसरी कन्या से संवाद कर रही थी- यू नो वी आर वैरी पुअर, वी हैव मारुति -800 ओनली यानी हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास सिर्फ मारुति 800 है।
महानगरों में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, जो अब मारुति -800 को गरीबों की कार बताते हैं या मोटरोला के सबसे सस्ते मोबाइल हैंडसेट, क्योंकि यह रसीद समेत करीब बत्तीस सौ का पड़ता है। यही वजह है कि इसे गरीबों का मोबाइल कहा जाता है।
25 रुपए का बर्गर इस हिसाब से गरीबों का बर्गर है और किसी धांसू सिनेमा हाल के सबसे सस्ते पचास रुपए के टिकट को गरीबों का टिकट बताया जा सकता है। गरीबों का स्तर इतना बढ़ गया हैं या फिर कार, बर्गर, मोबाइलों का स्तर गिर गया है।
यह सवाल महत्वपूर्ण है। इंडिया के माने बदल गए हैं या गरीब के माने बदल गए है या फिर विलासिता और आवश्यकता की वस्तुओं के माने ही बदल गए हैं। फ्रिज, टीवी को अब विलासिता की वस्तुओं में नहीं गिना जाता। फ्रिज, टीवी की गिनती अब निम्र मध्यम वर्ग की जरूरत के साज समान में होती है।
महानगर के मध्यमवर्गीय बंदे की बातों को सुनें, तो वह बताता है कि कार और मोबाइल तो अब आवश्यकता की जरूरतें हैं। विलासिता की नहीं। सो कार वाले अब विलासी की श्रेणी में नहीं आते।
विलासिता की वस्तुओं की प्रचलित परिभाषा के दायरे में अब फैशन डिजाइनरों द्वारा डिजाइन कपड़े, मंहगे कास्मेटिक्स, चमड़े के महंगे समान, महंगी घडिय़ां, जेवरात, महंगी शराब और महंगी कारें ही आती हैं।
पूरे विश्व में इस तरह के आइटमों का बाजार 80 अरब अमेरिकन डालर का है। इसका 30 प्रतिशत तो अकेले अमेरिका में ही है। यूरोप में इस बाजार का 38 प्रतिशत है। इसका करीब 35 प्रतिशत बाजार एशिया में है। भारत एशिया के तेजी से विकसित बाजारों में से एक है।
भारत में अब 1100 रुपए के मोजे, ह्यïूगो बास के 55000 के सूट, सात हजार की की चेन, नौ हजार की जीन्स उपलब्ध हैं। दस हजार के डिजाइनर कुरते उपलब्ध हैं और बिक भी रहे हैं। कालाहांडी भी इसी भारत में उपस्थित है और 55000 का सूट भी उपस्थित है। अपना- अपना इंडिया है, अपने- अपने आइटम हैं।
भारत जैसे बड़े देश के घटनाक्रम मेें पिछले कुछ सालों में यह साफ किया है कि किसी देश की आर्थिक स्थिति के सामान्यीकृत पैमाने स्थितियों को बह़ुत साफ तौर पर साफ नहीं कर सकते। एक अरब की जनसंख्या वाले देश में अगर एक लाख परिवार भी ऐसे हों, जिनकी सालाना आय बीस लाख रुपए या इससे अधिक हो तो यह भी अपने आप में बड़ा बाजार बनता है।
अब तो भारत में 10,3000 परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय बीस लाख रुपए या इससे ज्यादा है। भारत में करीब 24000 परिवार ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा है। इन परिवारों के बारे में कहा जा सकता है कि ये मिलकर भारत में अमेरिका का निर्माण करते हैं।
अमेरिका का मतलब है कि भरपूर उपभोग के अनंत अवसर। तमाम महंगे उत्पादों के मार्केटर इस अमेरिका पर नजर गड़ाए रहते हैं। पर मामला सिर्फ आय का नहीं है, संपत्ति का नहीं हैै। मामला मनोवृत्ति का भी है। उपभोग अपराध नहीं है, जमकर कमाना और फिर ऐश से लुटाना कोई खराब बात नहीं है।
धीमे- धीमे यह बात भारतीय समाज के बड़े वर्ग में बैठती जा रही है। वे दिन गए जब धन को लेकर विचित्र किस्म का गांधीवादी, समाजवादी रोमानी किस्म का भाव रहता था। अमीरी के साथ जो नैतिक अपराधबोध पहले उपस्थित होता था, अब वह गायब है।
आर्थिक नीतियों में समाजवादी नीतियों का दिखावा दिखावे के लिए भी नहीं होता। पहले अधिकांश फिल्मों में नायक गरीब होता था, गरीबों और गरीबी के पक्ष में होता था। अब मामला वैसा नहीं रहा। सारी फिल्मों का यशचोपड़ाकरण हो गया है। उच्च मध्यम वर्गीय नायक, जिसके लिए महंगे घर, महंगी कारें सहज उपलब्ध हैं।
यह अनायास नहीं हैै कि पंद्रह साल पहले तक हिट फिल्मों में गरीबी- अमीरी के अंतरद्वंद्व दिखाई पड़ जाते थे। अब मामला वैसा नहीं रहा। यश चोपड़ा प्रवृत्ति हिंदी फिल्मों की अब केंद्रीय प्रवृत्ति हो गयी है- टनाटन खाना-पीना और प्यार मुहब्बत।
इसी प्रवृत्ति के चलते अब संभव है कि कोई ग्रीटिंग कार्ड कंपनी पांच सौ रुपए का वैलेंटाइन कार्ड बेच लेती है, जो नौजवान इसे अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो आवश्यकता है, जो नौजवान इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यह सपना है, जिसे मौका मिलते वह पूरा करना चाहेंगे।
उपभोग के प्रति भारतीय समाज पर लंबे अरसे तक तमाम तक तरह के वैचारिक आध्यात्मिक दबाव काम करते रहे हैं। वे अब सिरे से अनुपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त गौरतलब यह है कि जो बच्चा अब से पंद्रह साल पहले दस बरस का था, वह अब पच्चीस बरस का है।
इस पीढ़ी के अधिकांश बच्चों के सामने किसी भी तरह का ऐसा वैचारिक, राजनीतिक माडल असरदार तरीके से पेश नहीं हुआ, जो धुआंधार उपभोग के प्रति एक नकार का भाव रखता हो, जैसे भाव पुराने समाजवादी माडल में पाए जाते थे।
सो इस पीढ़ी के समक्ष आवश्यकता और विलासिता की चीजों के बीच के फर्क का वैचारिक आधार अनुपस्थित है। जैसे ही आर्थिक आधार मजबूत होता है, ये पीढ़ी जमकर उपभोग करती हैं। यह अनायास नहीं है कि तमाम मीडिया इस नौजवान वर्ग को केंद्र में रखकर ही अपनी नीतियां तय कर रहा है, क्योंकि यही भविष्य का जोरदार उपभोक्ता वर्ग है।
उपभोग के प्रति वैचारिक नकार का भाव साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं के ध्वस्त होने के बाद पूरे विश्व में ही तिरोहित हो रहा है। सामूहिक मुक्ति के स्वप्न निजी उपलब्धियों की आकांक्षाओं द्वारा स्थानापन्न हो रहे हैं। निजी उपलब्धियां यानी उपभोग का लगातार बढ़ता स्तर।
लगातार विकसित होती तकनीक ने यह सुनिश्चित किया है कि विश्व के संपन्न लोग, वे चाहे किसी भी देश में हों, चुनिंदा ब्रांडों का उपभोग कर सकें। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में सबकी आय भले ही न बढ़ी हो पर कुछ वर्गों की आय में तो लगातार इजाफा हुआ है। इस आय का नए किस्म के उपभोग से सीधा रिश्ता है।
2002–2003 में करीब साढ़े पांच लाख कारें बिकीं। 2003–2004 के दौरान इस आंकड़े में दस फीसदी की बढ़ोत्तरी के आसार हैं यानी कार रखने की हैसियत वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों की आय में बढ़ोत्तरी हो रही है। इस स्थिति में नए किस्म के उपभोग की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं।
यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे एक अरब के देश में कुछेक लाख परिवारों की सालाना आमदनी भले ही बीस लाख से ऊपर हो, पर इसे तो पूरे देश के विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता है।
ठीक है कि इसे समग्र विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता, पर महंगे आइटम बेचने वाले कारोबारियों की चिंता देश के समग्र विकास की न होकर, अपने बाजार के विकास की है। वे इसमें सफल हो रहे हैं। वे भारत स्थिति अपने अमेरिका से प्रसन्न हैं। वे भारत में बनने वाले भविष्य के अमेरिका से प्रसन्न हैं, भारत का बांग्लादेश या भारत का इथियोपिया उनकी चिंता के दायरे में नहीं है और हो भी क्यों, अपने-अपने इंडिया अपने-अपने आइटम।